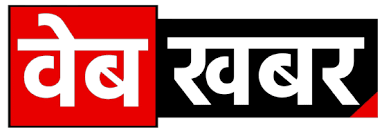विरोध में यदि विष का तड़का लग जाए तो वही होता है, जो संसद में हुआ। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने जिस आपत्तिजनक शब्द का केंद्र सरकार के लिए प्रयोग किया, वह केवल हंगामे का विषय नहीं है. वह चिंता और चिंतन, दोनों का मसला है। मोइत्रा ने जो कहा, वह नाजायज पैदाइश वालों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उनके द्वारा ‘नाजायज’ उस सरकार को कहा गया, जो पूरे जायज़ तरीके से लगातार दूसरी बार देश की सत्ता में आई है। तो भला आप किस तरह देश के जनमत को नाजायज वाली श्रेणी में ला सकते हैं? कैसे यह अधिकार माना जा सकता है कि इस तरह की बात कहकर पूरे लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया जाए?
कथनी और करनी, दोनों के लिहाज से ही अमर्यादा वाला माहौल दुखद रूप से अब आम बात हो चला है। राजनीति में तो खैर इस दिशा में प्रतिस्पर्द्धा मची हुई दिखती है। वह दौर अस्त हो चुका है, जब कहा जाता था कि सियासत में मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं। वहां अब परस्पर विरोध आत्मा को भेद देने वाले निम्न स्तर पर पहुंच गए हैं। मोइत्रा अपने कहे पर कायम हैं। उनका कहना है कि उन्होंने वही कहा, जो सही है। वह एक वीडियो का हवाला देकर दलील दे रही हैं कि और भी सांसद इस तरह की भाषा का प्रयोग कर चुके हैं। एक सवाल याद आता है। यदि जूता आपको काटता है तो क्या आप जूते को काटने लगेंगे?
दरअसल केंद्र सरकार पर विपक्ष का गुस्सा अब तेजी से विकृत रूप लेने लगा है। इसकी कई वजह हो सकती हैं। सरकार को मुद्दों के आधार पर घेरने की असफलता इनमें से एक प्रतीत होती है। तमाम विरोधी कोशिशों के बाद भी वर्तमान भारत का विदेशों में बढ़ता कद भी इसका कारण बन गया लगता है। पश्चिम बंगाल में किसी समय अतित्व-विहीन दिखने वाली भाजपा आज वहां दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, हो सकता है कि मोइत्रा का गुस्सा इससे जुड़ा हुआ हो। वजह चाहे जो हो, लेकिन जो हुआ उसे किसी भी तरह से सही नहीं कहा जा सकता। फिर सदन में तो हर बात के लिए प्रक्रिया और व्यवस्था सुनिश्चित की गयी हैं। यदि कोई बात वाकई नाजायज है, तो उसे लेकर आगे बढ़ने के लिए तमाम नियम और समितियां अस्तित्व में हैं। लेकिन प्रक्रियाओं को परे रखकर केवल ऐसी सतही प्रतिक्रियाओं से सुर्खी बटोरने वाली मानसिकता का भला क्या किया जाए?
फ़िक्र की बात यह कि अब इस तरह के आचरण पर रोक लगाने के सारे मार्ग बंद होते दिख रहे हैं। आप लाख कोशिश कर लीजिए। कुछ शब्दों को ‘असंसदीय’ वाली काल कोठरी में बंद कर दीजिए, लेकिन इसकी काट में हजारों ऐसे पिटारे खुल जाते हैं, जिनके भीतर वैचारिक मलिनता वाले भयावह सांप बैठे हुए हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि इस आचरण के पैरोकार खुद ही अपने भीतर कोई बदलाव करना नहीं चाहते हैं। उन्होंने असंसदीय और अशालीन होने को अपनी यूएसपी मान लिया है। एक साक्षात्कार याद आ गया। कंधे पर मैला ढोने की कुप्रथा से सभी परिचित हैं। भोपाल के एक पत्रकार ने उस समय भी यह काम करने वाली महिला से बात की थी। उसने जवाब में गर्व के साथ कहा था, ‘यह मैला हमारे लिए सोने (धातु) की तरह है। इसे भला कैसे खुद से अलग कर दें?’ क्या बदजुबानी की तोहमतों को किसी आभूषण की तरह अपने श्रृंगार का माध्यम मानने वाले भी उस महिला की ही तरह आचरण नहीं कर रहे हैं? संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा गया है और यदि वहां ही इस तरह के कृत्यों का प्रदर्शन किया जाएगा, तो फिर विधानसभा से लेकर पंचायतों की सभा और चौक-चौराहों से लगाकर आम घर की बैठक तक की शालीनता पर इसका विपरीत असर होना तय है। लेकिन क्या कोई इस बात को समझेगा?
आज के संवाद का हर पैराग्राफ प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ समाप्त हुआ है। क्योंकि ऐसे विषयों पर अब केवल प्रश्न उठाने जैसी स्थिति ही रह गयी दिखती है। फिर भी इस उत्तर की तलाश तो की ही जानी होगी कि ऐसे सवालों के अकेलेपन को दूर करने वाले उत्तर कभी मिल भी सकेंगे या नहीं?